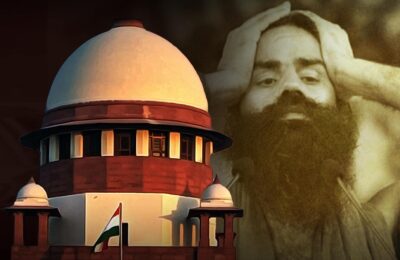एक सच्ची नज़्म : उठ जाग मुसाफ़िर भोर भई
Feb 05, 2019
उठ जाग मुसाफ़िर भोर भई
रातों की साँसें थमती थी,
सुबह का अंधेरा हर दर पर,
आ आ के दस्तक देता था,
सूरज तो अभी था परदे में,
लाली भी उभर न पाई थी,
पिछले की हवाएं चलती थी,
कुछ ठंढी सी कुछ शरमाती,
और नींद भी बाहें सिमटा कर,
ज़ेहनों से लिपटी रहती थी,
ऐसे में बंजारा आता,
अपनी धुन में गाता जाता,
उठ जाग मुसाफ़िर भोर भई।
वह बचपन के दिन क्या दिन थे,
न फ़िक्र कोई न ही डर था,
अपनी दुनियां थी बहुत बड़ी,
यानी अपना घर आंगन था,
बेले की महक जूही की गमक,
पूरे घर में फैली रहती,
और शाम ढले रजनी गंधा,
कुएं के बग़ल से सज धज कर,
चुप चाप सेहन की गोदी में,
अपना एहसास कराती थी,
हम शाम ढले खाना खा कर,
बिस्तर से इश्क़ लड़ाते थे,
जब प्यार भरी झिड़की मिलती,
मुंह ढांप के फिर सो जाते थे,
ख़्वाबों ने अगर डेरा डाला,
तो जी भर के मुस्काते थे,
और रूप अगर बदला उसने,
तो नींद में ही डर जाते थे,
आवाज़ पड़ी जब कानों में,
तो हंस कर नींद चली जाती,
उस बंजारे की आवाज़ें,
दीवारों से टकराती थीं,
उठ जाग मुसाफ़िर भोर भई।
न जाने कब वह खाता था,
कब जगता था कब सोता था,
किस ताने से किस बानें से,
झीने कपड़ों को बुनता था,
जब भी चाहा उसको देखूँ,
थोड़ा जानूं थोड़ा परखूँ,
पर मुझे नज़र न आता था,
अंधियारे में खो जाता था,
पर आवाज़ों की डोली पर,
साज धज कर वह बैठा रहता,
अपनी धुन में गाता रहता,
उठ जाग मुसाफ़िर भोर भई।
कितने दिन रातें बीत गईं,
ऐसे ही बरसों गुज़र गए,
गिनते गिनते सब भूल गए,
कितने आये और चले गए,
बसती की रंगत बदल गई,
छप्पर खपरे सब ख़ाक हुए,
बादल की चमक बिजली की कड़क,
अपने ग़म से ग़मनाक हुए,
अब पक्के घरों का जंगल था,
मंगल की जगह इक दंगल था,
पैसों के कबूतर लड़ते थे,
ऐसे में अपने मिलते नहीं,
गुड़ भी पानी में घुलते नहीं,
शरबत में कड़ुवाहट देखी,
और छाछ उबलता रहता था,
गावँ में भीड़ इकट्ठा थी,
फिर भी सन्नाटा पसरा था,
ऐसे में अपने गावँ गया,
न आंगन था न बेला था,
न रात की रानी को देखा,
कुएं में कूड़ा करकट था,
शकलें भी नई नई दिखतीं,
हां क़ब्र की बसती बढ़ी हुई,
न जाने कितने लाला रुख़,
की हसती उसमें धंसी हुई,
इक आस लिए हम सोये थे,
मीठे सपनों में सोए थे,
आ कर कोई तो गाए गा,
उठ जाग मुसाफ़िर भोर भई।
सूरज की किरनों ने आ कर,
मुंह पर चिंगारी रखने लगी,
चमड़ी की जलन से भीतर तक,
बस आग का दरिया बहता था,
दुबकी सी रूह के अंदर भी,
अब भी इक आस का डेरा था,
वह बंजारा फिर आए गा,
अपना पैग़ाम सुनाए गा,
भूला वह गीत सुनाए गा,
उठ जाग मुसाफ़िर भोर भई।
जो जागत है ऊ पावत है।
जो सोवत है ऊ खोवत है।

मेहदी अब्बास रिज़वी
” मेहदी हल्लौरी “